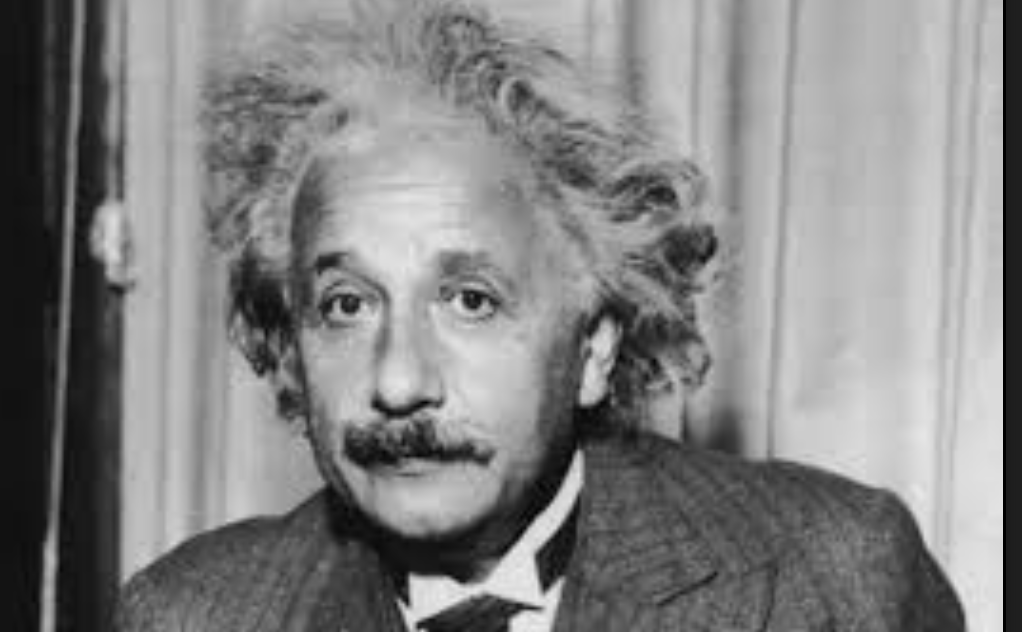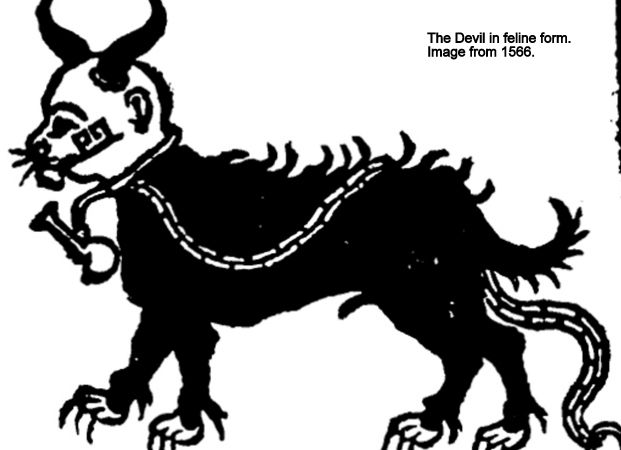भारत में दिल्ली के आसपास झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाली बेसहारा प्रवासी महिला सईदा एक्स ने 30 वर्षों तक 50 से अधिक व्यवसाय किए।

डेनिम के धागे काटने, खाना पकाने और बादाम छीलने के अलावा, वह चाय की छलनी, दरवाज़े के हैंडल, तस्वीरों के फ्रेम और खिलौने वाली बंदूकें भी सिलती थीं। गहने और मोतियों की कढ़ाई के साथ-साथ, वह स्कूल बैग पर कढ़ाई भी करती थीं। उनकी मात्र 25 रुपये (30 सेंट; 23 पेंस) की कमाई, 1,000 खिलौने वाली बंदूकें बनाने की उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा थी।
लेखिका नेहा दीक्षित द्वारा लिखित "द मेनी लाइव्स ऑफ़ सैयदा एक्स" सैयदा और उनके परिवार की कहानी है, जो 1990 के दशक के मध्य में पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में धार्मिक अशांति के बाद दिल्ली आकर बस गए थे। यह पुस्तक, जो एक दशक में लिए गए 900 से ज़्यादा साक्षात्कारों पर आधारित है, एक ऐसी महिला भारतीय कामगार के कठिन जीवन पर प्रकाश डालती है जो अपने घर के आराम से अपना काम करती है।
सुश्री दीक्षित की पुस्तक में भारत की गुमनाम महिला गृह-आधारित कामगारों के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। भारत में किसी व्यक्ति को गृह-आधारित कामगार तभी माना जाता है जब वह अपने घर या किसी अन्य निर्दिष्ट स्थान से किसी व्यवसाय के लिए वस्तुएँ या सेवाएँ तैयार करता है, भले ही वह व्यवसाय आवश्यक उपकरण या सामग्री प्रदान करता हो या नहीं। इस वर्गीकरण को 2007 में ही एक अलग श्रमिक वर्ग के रूप में कानूनी मान्यता दी गई थी।
इसका एक उदाहरण पतंग बनाने वाला है; भारत में घर से काम करने वाले 41 मिलियन लोगों में से लगभग 17 मिलियन महिलाएं हैं
कृषि को छोड़कर, भारत की अधिकांश कामकाजी महिलाएँ (80% से अधिक) किसी न किसी प्रकार की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में लगी हुई हैं, जिनमें से सबसे आम है घर से काम करना। लेकिन इन महिलाओं की मदद के लिए कोई कानून या कार्यक्रम मौजूद नहीं है।
अनौपचारिक नौकरियों में महिलाओं की मदद करने वाली एजेंसी, विएगो के अनुसार, 2017 और 2018 में घर से काम करने वाले 4.1 करोड़ भारतीयों में से लगभग 1.7 करोड़ महिलाएँ थीं। कार्यबल में लगभग नौ प्रतिशत महिलाएँ थीं। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में उनकी शहरी आबादी तेज़ी से बढ़ी है। इस विषय पर व्यापक शोध कर चुकी इतिहासकार इंद्राणी मजूमदार कहती हैं, "घर से काम करने वालों का रुझान शहरी क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है।"
ये महिलाएँ गरीबी, असुरक्षा और बेवफ़ा पतियों के खिलाफ़ एक कठिन संघर्ष करती हैं क्योंकि उनके पास सामाजिक सुरक्षा और अन्य प्रकार के संरक्षण का अभाव है। वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने और खुद को और अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करती हैं। उनके घरों में मानसून के दौरान जलभराव के कारण उन्हें दी गई सामग्री बर्बाद हो जाती है, और ये महिलाएँ जलवायु परिवर्तन की कीमत भी भुगतती हैं, आजीविका खोती हैं और घाटे में रहती हैं।
अर्थशास्त्री सोना मित्रा का अनुमान है कि भारत की 751,300 महिला विनिर्माण श्रमिक अपने घरों में आराम से अपना काम करती हैं। वे कहती हैं, "इन महिलाओं को स्व-रोज़गार वाली महिलाओं की सूची में रखा गया है और अक्सर इन्हें नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है।"
सुश्री दीक्षित की विचलित करने वाली कहानी में सईदा एक्स और घर से काम करने वाली अन्य महिलाओं को उत्पीड़न और लाचारी के प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया है। उनकी सेवाओं के लिए इतनी कम कीमत कौन तय करता है, यह एक रहस्य बना हुआ है। कोई भी आपको किसी भी तरह का मार्गदर्शन, शिक्षा या संसाधन नहीं देता। जब काम सीखने की बात आती है, तो ये महिलाएँ पूरी तरह से एक-दूसरे पर निर्भर रहती हैं।
सुश्री दीक्षित ने कहा कि समाचार चक्र से अवगत रहना अक्सर काम पाने का एक अच्छा तरीका है।
1997 में, जब कल्पना चावला अंतरिक्ष में पहुँचने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बनीं, महिलाओं ने प्लास्टिक की गुड़ियों को हाथ से सिले सफ़ेद स्पेससूट पहनाए। उन्होंने 1999 के क्रिकेट विश्व कप के लिए सैकड़ों सस्ते फुटबॉल सिले। 2001 में दिल्ली में "बंदर आदमी" की एक अफवाह फैल गई, जिसके कारण उस जीव जैसे दिखने वाले मुखौटों की माँग बढ़ गई, और ये मुखौटे ट्रैफिक चौराहों पर बेचे जाने लगे। चुनाव के मौसम में इस्तेमाल के लिए उन्होंने पार्टी के झंडे, चाबी के छल्ले और टोपियाँ बनाईं। स्कूल वापसी के लिए उन्होंने क्रेयॉन, स्कूल बैग और जिल्दबंद किताबें तैयार कीं।
1990 के दशक तक रेडीमेड परिधान व्यवसाय में अनेक कार्य घरेलू श्रमिकों को आउटसोर्स किये जाते थे।
इसके अलावा, कई महिलाओं को महीने में 20 दिन से ज़्यादा घर से काम करने वाली नौकरियाँ ढूँढ़ने में मुश्किल होती है। सुश्री दीक्षित के लेख के अनुसार, केवल वे लोग ही आसानी से रोज़गार पा सकते हैं जो कीमतों पर मोलभाव नहीं करते या ज़्यादा सवाल नहीं पूछते, जो अपने औज़ार खुद लाते हैं, जो हमेशा समय पर काम पहुँचाते हैं, जो आपात स्थिति में कभी अग्रिम राशि या सहायता नहीं माँगते, और जो देर से भुगतान को संभाल सकते हैं।
सुश्री मजूमदार के अनुसार, रोज़गार की प्रकृति में बदलाव ने घरेलू महिला कामगारों का जीवन और भी अनिश्चित बना दिया है। 1990 के दशक तक रेडीमेड कपड़ों के व्यवसाय में कई काम घर से काम करने वाले लोगों को आउटसोर्स किए जाते थे। 1990 का दशक एक महत्वपूर्ण मोड़ था क्योंकि कढ़ाई सहित कई निर्माण प्रक्रियाओं में मशीनों ने मानव श्रमिकों की जगह लेना शुरू कर दिया और निर्माताओं ने कामों को घर के अंदर ही स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। उनके अनुसार, "घर से काम करना बहुत अस्थिर हो गया।"
2019 में, ILO ने अनुमान लगाया कि दुनिया के 7.9% श्रमिक, या 260 मिलियन व्यक्ति, 118 देशों के घरों के सर्वेक्षण के आधार पर घर से काम करते हैं।
ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के शोध के अनुसार, जब स्थानीय सरकारें और ट्रेड यूनियनें सफलतापूर्वक एक साथ काम करती हैं, तो श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा की जा सकती है और उप-अनुबंधित या घर-आधारित नौकरियों में कार्य स्थितियों की निगरानी की जा सकती है।
एएफपी 15 जुलाई, 2018 को, भारत की एक मुस्लिम महिला अपने घर पर कागज़ के थैले धोती है और उन्हें इलाहाबाद में व्यापारियों को बेचती है। - एएफपी 15 जुलाई से, उत्तर प्रदेश सरकार ने पॉलिथीन बैग और अन्य आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के सामानों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है।
भारत में ऐसे उदाहरण बहुत कम हैं। स्व-रोज़गार महिला संघ (सेवा) एक सदस्यता-आधारित संगठन है जो अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाली निम्न-आय वर्ग की महिलाओं को एक साथ लाता है, जो 52 वर्षों से अस्तित्व में है। घर-आधारित कामगारों के लिए माइक्रोफाइनेंस और स्वयं सहायता संगठन उनके लिए उपलब्ध हैं। सुश्री मजूमदार ज़ोर देकर कहती हैं, "लेकिन रोज़गार के मामले में इन योजनाओं से उन्हें वास्तव में कोई मदद नहीं मिली है।"
दिल्ली में महिलाओं के एक समूह ने 2009 में अन्य मांगों के अलावा, अधिक वेतन और बादाम की सफाई व छिलका उतारने के काम से अधिक छुट्टी की मांग को लेकर हड़ताल की थी। (उन्होंने 12-16 घंटे तक 23 किलोग्राम का बैग साफ किया और 50 रुपये प्रति बैग प्राप्त किए।) साल के सबसे व्यस्त समय में, बादाम प्रसंस्करण उद्योग हड़ताल के कारण ठप हो गया था।
भारतीय राज्य तमिलनाडु की सामाजिक वैज्ञानिक के. कल्पना ने चेन्नई के अप्पलम (पापड़म) उद्योग में महिला उपठेकेदारों के अधिकारों के लिए संघर्ष का दस्तावेजीकरण किया है और बताया है कि किस प्रकार उन्होंने उन सरकारी संस्थाओं पर अपनी पकड़ बनाई, जिन्होंने पहले उनकी मांगों को नजरअंदाज किया था।
न तो सईदा एक्स और न ही उनके साथी भाग्यशाली रहे। सुश्री दीक्षित लिखती हैं, "अगर वह कभी किसी बीमारी का इलाज कराने या अपने बच्चों की देखभाल के लिए छुट्टी लेतीं, तो कोई और अनाम प्रवासी उनकी जगह लेने के लिए लड़ता।" एक नौकरी से दूसरी नौकरी और एक घर से दूसरे घर जाते हुए, उनके जीवन में केवल विस्थापन और दुख ही स्थिर रहे।